एक पागल आदमी की चिट्ठी-सी विकल कविता – विमलेश त्रिपाठी की दो लम्बी कविताओं पर रसाल सिंह का लेख
विमलेश त्रिपाठी समकालीन समय के सर्वाधिक संभावनाशील और
विश्वसनीय युवा साहित्यकार हैं। उन्होंने हम बचे रहेंगे, एक देश और मरे हुए लोग (कविता-संग्रह), अधूरे अंत की शुरुआत (कहानी-संग्रह) और कैनवास पर प्रेम (उपन्यास) नामक
रचनाओं के जरिए अपनी अलग पहचान बनायी है। उनके लिए ‘लिखना
जीने का और जीना लिखने का पर्याय’ और पारस्परिक स्रोत हैं।
सहज और सरल भाषा में अपने कथ्य और सर्जनात्मक चिन्ताओं को सम्प्रेषित करना उनकी खासियत
है। वे युवा सर्जनात्मकता की एक ऊर्जस्वी और भविष्यधर्मी आवाज हैं।
विमलेश
त्रिपाठी की कविताएं ‘एक देश और मरे हुए लोग’, ‘एक पागल आदमी की चिट्ठी’ और ‘हम
बचे रहेंगे’ आदि, वास्तव में उदारीकरण
के बाद के भारत देश और भारतवासियों की मरणासन्नता का आलोचनात्मक आख्यान हैं। गल्प
के शिल्प में लिखी गयीं ये कविताएं भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप ‘भारत’ और ‘भारतवासियों’
के क्रमशः मरते चले जाने का ब्यौरा देती हैं। सन् 1991 के आसपास अपनाई गयी ‘नई आर्थिक नीति’ ने न सिपर्फ गाँव-गिरांव को उजाड़ दिया बल्कि पारिवारिक संबंधें को भी
सिकुड़ा दिया। लोगों के सामाजिक बोध् और नैतिक चेतना में गुणात्मक गिरावट आई।
मनुष्य यकायक ‘सामाजिक प्राणी’ से एक
व्यक्ति मात्रा में तब्दील हो गया। वह मनुष्य से क्रमशः ऐसा ‘पशु’ बन गया जिसे जैसे-तैसे तृप्तकाम होना है। यह
तृप्ति किन शर्तों पर और क्या कुछ गँवाकर मिल रही है, यह
प्रश्न उसे तनिक भी विचलित नहीं करता बल्कि कहना चाहिए कि ऐसे सवालों के बारे में
सोचने की उसे न तो जरूरत है और न ही उसके पास पफुरसत है। नयी सदी में प्रवेश करते
ही सूचना-तकनीक क्रान्ति और उपभोक्तावादी हवश ने मनुष्य को अपने पंजों में दबोच
लिया है। अब उसके पास अपने आस-पड़ोस, परिवार, मित्रों, संबंधियों और देश-समाज की सुध-बुध लेने का
समय और चिन्ता नहीं बची है।
मृतात्माओं
को पुनर्जीवित करने के संकल्प के साथ लिखी गयी विमलेश त्रिपाठी की कविताएं
सामूहिकता, सामाजिकता और नैतिकता की मृत्यु का प्रलाप मात्रा
नहीं अपितु पश्चिमीकरण, तकनीकीकरण और बाजारीकरण के खतरों की
सजग सूचना हैं। ये तीनों माया के उत्तरआधुनिक ‘तिरगुन फाँस’
हैं, जिनमें उसने भारत जैसे अविकसित, अल्पविकसित देशों को फाँस लिया है और आजादी के 65-70
साल बाद भी आजाद नहीं होने दिया है। नव्य-पूँजीवाद और नव्य-उपनिवेशीकरणजनित गुलामी
हमारी अनिवार्य पारिस्थितिकी है। इस मानसिक गुलामी ने मनुष्य के सोचने-समझने की
क्षमता को नष्ट करके उसे मृतप्राय बना दिया है। आज वह अपने जीवन और अपनी भौतिक
जरूरतों को पूरा करने की जुगत में अपनी जड़ों से कटता जा रहा है। चरम उपभोग और
विलासिता की वस्तुओं का संग्रह ही उसका एकमात्रा ध्येय है। इस वस्तुवाद ने उसे
बौद्धिक रूप से पूरी तरह विपन्न करके चरम सांस्कृतिक संकट पैदा कर दिया है। विमलेश
त्रिपाठी इन्हीं तमाम संकटों की पड़ताल करते हैं और उनका एक यकीनतलब विवरण हमें
देते हैं। आदिवासी, स्त्री, किसान,
दलित, ईमानदार और स्वाभिमानी मनुष्य, ये सब-के-सब किस प्रकार हमारे ‘लोकतांत्रिक देश’
में अप्रासंगिक और अनुपयोगी होते जा रहे हैं, किस
प्रकार बारीक-से-बारीक चक्रव्यूह रचकर उनका संहार किया जा रहा है, ये सब सवाल लगातार उनकी चिंता के केन्द्र में हैं। पूरी की पूरी प्रशासनिक
मशीनरी इन लोगों को ठिकाने लगाने की दिशा में सक्रिय और संकल्प नजर आती है। एक
लोकतांत्रिक देश को जहाँ आम आदमी के हित और हक के लिए काम करते हुए ‘लोक कल्याणकारी राज्य’ होना चाहिए था, वहाँ वह सिर्फ चुनिन्दा लोगों के लिए काम कर रहा है-
‘‘इतिहास के कई रंग हो सकते हैं
लेकिन पागल आदमी की चिट्ठी में
इतिहास का रंग काला ही होता है अक्सर
और यह गौर करने लायक बात है
कि उसकी चिट्ठी में
इतिहास लिखकर उस पर स्याही पोत दी गई होती है
……………………………………………..
वे साजिशें लिखी होती हैं
जिसके कारण पैंसठ साल बाद भी
इस देश के एक अरब से अध्कि लोग
गुलाम और मरे हुए लोगों की तरह
हरकत करते दिखते हैं
पागल आदमी की चिट्ठी में
रंग नहीं लिखा होता
सिपर्फ खून के ध्ब्बे लिखे होते हैं।’’
उनकी कविता
समकालीन भारत में सोचने-समझने और अपनी बात को खुलकर रखने की गुंजाइश के लगातार
खत्म होते चले जाने की त्रासदी का बयान है-
‘‘अपने ही देश में सच बोलना मना
सच सोचना मना
सच को सच की तरह लिखना मना
छुप-छुप कर डर-डर कर जीना
मना मना मना जिंदा रहना’’
आज स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वतंत्र आचरण की कोई जगह इस देश में नहीं बची।
पालतू और पूँछ हिलाने वालों की पूछ है। इस देश में राजमाता से लेकर राजा तक सब मरे
हुए लोग हैं और अपनी लाश ढोने को अभिशप्त हैं। कहीं असहमति, विरोध्
या विद्रोह की जगह नहीं। असहिष्णुता, आक्रामकता और उन्माद का
बोलबाला है। जिन्दा व्यक्तियों, वस्तुओं और तर्कों को सबसे
बड़ा खतरा मानकर संगठित तरीके से उनका शिकार किया जाता है। जो गूँगे-बहरे, मुंडी हिलाने वाले और पिछलग्गू हैं, उन्हें तरह-तरह
से पुरस्कृत और प्रतिष्ठित किया जाता है। मनुष्यता की अवमानना और मनुष्य के
अमानवीकरण का धंधा जोरों पर है-
‘‘यह ढोल नगाड़ों का समय था
खाप पंचायतों का समय था
राजनीति का समय था
मक्कारी और बेशर्मी का समय था
इस समय सबसे अधिक होड़
सबसे कम आदमी रह जाने के लिए थी’’
सबको एक ही साँचे/खाँचे में ढालने की साजिशें चलती रहती
हैं – अनवरत्। सच बोलने वाले और सही सोचने वाले अपने ही देश में निर्वासित और
उपेक्षित हैं क्योंकि न सोचने वालों और न बोलने वाले मृतकों का बोलबाला और वर्चस्व
है-
‘‘एक पहले से मरा हुआ
गाता देशभक्ति के गीत
एक सदियों का मरा आदमी
ईश्वर और मुक्ति के उपाय पर
करता प्रवचन
मरे हुए लोग मुक्ति के लिए
लगाते भीड़ उसके आस-पास
मरे हुए लोगों का बढ़ रहा कारोबार
एक देश जहां मुर्दे लोग सबसे अधिक ताकतवर
जिंदा लोगों को भेजा जा रहा जेल
चढ़ाया जा रहा सूली पर
उन्हें मारने के लिए की जा रहीं
तरह-तरह की साजिशें’’
स्वार्थी, अहंकारी और पाखण्डी लोगों के लिए ‘रामराज्य’ है। उनके लिए अनेक अवसर और संभावनाएं हैं। झूठ, फरेब
और मक्कारी हमारे समय की अनिवार्य जीवन-स्थिति है। मरी हुई आत्मा वाले तमाम बुद्धिजीवी,
राजनेता, कलाकार, पत्राकार,
अपफसर, संत-महंत, मंत्री-संत्री
और यहाँ तक कि राजा स्वयं मुखौटे लगाये घूम रहे हैं और ऐसी स्थितियाँ बना रहे हैं
कि हर किसी को मुखौटा लगाना पड़ रहा है। इन मुखौटों के पीछे एक से एक छंटे हुए
गुण्डे, बदमाश, बलात्कारी, व्यभिचारी, घोटालेबाज, दगाबाज
छिपे हुए हैं। विमलेश त्रिपाठी अपनी कविताओं के माध्यम से इनके मुखौटों को नोंचकर
हमें उनकी वास्तविकता से परिचित कराते हैं। वे नयी सदी में धर्मतंत्र, राजनीति-तंत्र और अर्थतंत्र की आपसी और अवैध साँठ-गाँठ का पर्दाफाश करते
हैं-
‘‘उसे अमर होना है इतिहास में नाम दर्ज कराना है
हे नाथ क्षमा करना
वही करता भ्रष्ट सब काम
उसके चेहरे पर कई चेहरों की पर्तें
जिनका जरूरत के मुताबिक
करता इस्तेमाल
यह देश उसे ही मानता है आजकल
सभ्य नागरिक
शिष्टजन
अध्यापक
वैज्ञानिक
राजनीतिज्ञ
समाजशास्त्री
भाषाविद्
इत्यादि…..’’
ये कविताएं
समकालीन समय में मनुष्य के नैतिक-बोध, अन्तरात्मा की आवाज और
विवेक-चेतना की मृत्यु की विवरणिका हैं। ‘मरने के बाद आदमी
कुछ नहीं सोचता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, कुछ न सोचने और न बोलने से आदमी मर जाता है’ कहकर
वरिष्ठ कवि उदय प्रकाश जिन्दा मुर्दा आदमी की पहचान प्रस्तावित करते हैं। मूल्य
निरपेक्षता, रणनीतिक तटस्थता, चाटुकारिता,
स्वार्थपरता, अंधनुकरण-वृत्ति, आत्मस्पफीति, प्रदर्शनप्रियता और कायर अकर्मण्यता ने
आज के आदमी की आत्मा को खाली और खोखला बना डाला है। आज के भारत में मनुष्य-भाव और
अभिव्यक्ति-स्वातंत्रय की शवयात्रा निकल रही है। आत्मजीविता, असवरवाद और आत्मकेन्द्रिकता ने मनुष्य की आत्मा को मृतपाय कर दिया है।
विमलेश त्रिपाठी की यह कविता इसी संकट के गहराने की चिंता को व्यक्त करती है।
समकालीन मनुष्य जीवन की वास्तविकताओं से मुँह चुराकर अड़ोस-पड़ोस, परिवार-रिश्तों से कटकर ‘फेसबुक फ्रेन्ड्स’ के सहारे जी रहा है। वह आभासी, ओढ़ी हुई, पालिश्ड और परतदार छवियों को ही जीवन का सच मान रहा है। ये ऐसी ही अनेक
सच्चाइयों से उद्वेलित कविताएं हैं।
‘एक देश और
मरे हुए लोग’ नामक लंबी कविता को पढ़ते हुए स्मृति में
मुक्तिबोध की कालजयी कविता ‘अंधेरे में’ बराबर कौंधती है। ‘अंधेरे में’ की तर्ज पर ‘एक देश और मरे हुए लोग’ 21वीं सदी के भारत की स्वप्नहीनता, मानसिक पराधीनता,
आत्मजीविता और अवसरवाद का पता देती है। नयी सदी में बिगड़ते/मरते एक
देश की विस्तृत व्यथा-कथा इस कविता में मौजूद है। मानसिक गुलामी, धूर्तता, पाखण्ड और प्रपंच जीवन जीने की और आगे
बढ़ने की अनिवार्य शर्त बन गये हैं। जो दिन के उजाले में और सार्वजनिक जीवन में
नैतिकता की जितनी ज्यादा उल्टी करता है, वह रात के अंधेरे
में और व्यक्तिगत जीवन में उतना ही बड़ा ‘खूंखार दैत्य’
है। आज डिग्रियाँ, नौकरियाँ, ठेके, टिकटें, पुरस्कार सब कुछ
‘मृतात्माओं’ को दिया जा रहा है। जो
जिन्दा हैं, वे तिल-तिल मरने या फिर तिरस्कृत-बहिष्कृत होने
के लिए अभिशप्त हैं। यह कविता समकालीन भारत की वंचना का ब्यौरा देती है। ऐसे
अंधेरे समय में कवि को महात्मा गाँधी, विनाबा भावे, जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे, निराला और मुक्तिबोध जैसे जिन्दा लोगों की रह-रहकर याद आती है जिन्होंने
अपना देश तो बनाया पर घर नहीं-
‘‘कहते हैं
वह इतिहास से बचकर छुपते-छुपाते
चला आया एक आदमी था
जो वर्तमान में गाता घूम रहा था
और भविष्य की ओर देखते हुए
जार-जार रोता था
उसकी कथरी में असंख्य गीत थे
उसके दिमाग में कहीं और ज्यादा
इतने कि उससे एक देश बनाया जा सके
उसके गीत घर तो न बना सके
लेकिन देश बना सकते थे’’
आज गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी है। देश को बिगाड़कर, खुद की आत्मा को मारकर, पीढि़यों के
भविष्य को रौंदकर अपना ‘घर’ भरने की धुन
‘मृतात्माओं’ पर सवार है। लोग
व्यक्तिगत सुख-सुविधा के दायरे में सिमट-सिकुड़ गये हैं। उनकी आत्मा का आयतन बेहद
कम हो गया है। यह बात विमलेश त्रिपाठी को लगातार व्यथित और बेचैन करती है। इसलिए
वह सुषुप्त चेतना को जगाना चाहते हैं, मृतात्माओं में प्राण
पफूँकना चाहते हैं। वे मानसिक गुलामी और स्वार्थपरता को निरस्त करके एक स्वतंत्रा
एवं स्वस्थ सोच और सामूहिक-सामाजिक बोध् से समन्वित मनुष्य-समाज देखना चाहते हैं।
वे भौतिक वस्तुओं के संग्रह और असीमित विलासिता के बरक्स सब बच्चों के लिए हवा,
पानी और रोटी की जरूरत को रेखांकित करते हैं। वे संतुलित और
सार्वजनीन विकास की प्रस्तावना करते हैं जिससे दूर-दराज के ग्रामीण-किसान, आदिवासी, दलित और स्त्रियाँ भी भारत को अपना देश मान
सकें। उसकी राष्ट्रीयता से जुड़ सकें –
‘‘1857 की क्रान्ति को एक शोकेस में सजाकर
धूप और अगरबत्ती दिखा रहे हैं कुछ लोग
बिरसा मुण्डा बिरसा मुण्डा
चिल्ला रहा है एक आदिवासी
एक लड़की लक्ष्मीबाई की तस्वीर
और झण्डा लेकर खड़ी है
पुरुषों की सदियों पुरानी परंपराओं के खिलापफ
मंच पर पता नहीं कितने समय से
चल रहा है यह दृश्य
यह नाटक रुकने का नाम ही नहीं लेता
जब कि इस देश को आजाद हुए
हो गया पैंसठ साल से ज्यादा’’
अभी तो भारत
एक बीमार, मरणासन्न और खण्डित राष्ट्रीयता का देश बन गया है।
रघुवीर सहाय ने ‘राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता
है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुन हरचरना गाता है’ कहकर अपने ही देश में अजनबी और उपेक्षित वंचित तबकों की पीड़ा को आवाज दी।
विमलेश त्रिपाठी भी फटा सुथन्ना पहने हुए भूखे पेट वाले करोड़ों ‘हरचरनाओं’ की दुखगाथा कहते हैं। अपने जल, जंगल, जमीन और जज्बात से करोड़ों आदिवासियों-किसानों
का विस्थापन कवि के मन में आक्रोश भरता है। इस आक्रोश की आवेगमयी अभिव्यक्ति ‘एक देश और मरे हुए लोग’ है। वह इस विडंबना को भी
उभारते हैं कि 65-70 साल पहले आजाद हुए देश में आज भी मुक्ति
गीतों की जरूरत है-
‘‘एक नदी है मेरी धमनियों में बहती
एक गांव है मेरे फेंफड़े में हांफता
एक औरत है जो मेरी परछाई है
एक-एक शब्द मेरी सांस हैं
एक-एक कविता मेरा जीवन…
एक गुमनाम कवि मैं
अंततः
एक चौराहे पर खड़ा होकर
जोर-जोर से चिल्लाना चाहता हूं
देश
देश और लोकतंत्र
कि कविता कविता
और कविता…।’’
वस्तुतः कवि का इशारा सामाजिक-आर्थिक पराधीनता की ओर है।
हालांकि, राजनीतिक आजादी भी ‘शोकेस’ में सजाने और दिखावे की चीज भर ही है। स्वतंत्रता,
समानता और बंधुत्व जैसे स्वाधीनता आन्दोलन के जीवन-मूल्य और नारे
संविधान नामक किताब में मरणासन्न पड़े हैं। विमलेश त्रिपाठी मनुष्य के मरते चले
जाने के कारणों की पड़ताल करते-करते हमारे ‘पवित्र धार्मिक
ग्रंथों’ का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं और स्थापित
करते हैं कि इन धार्मिक ग्रंथों ने भी स्वतंत्र चिंतन की संभावनाओं को बराबर कम
किया है। मनुष्य को असहिष्णु और उसकी मानसिकता को संकुचित किया है।
विमलेश
त्रिपाठी की कविता हमारे समय के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रदूषण और आर्थिक-राजनीतिक
भ्रष्टाचार का मुकाबला करने को संलग्न होती है। उनको कविता और जिन्दगी की जीत में
गहरा यकीन है-
‘‘देश और देश और देश के बीच
मरे हुए और मरे हुए लोगों के बीच
कथा और हकीकत के बीच
बचे हुए कुछ जिंदा शब्द
हंस रहे पूरे आत्मविश्वास के साथ
और बन रही है कहीं
कोई एक लंबी कविता।’’
कवि की स्थापना और मान्यता है कि ‘विकल्पहीन नहीं है दुनिया।’ आज
उच्छृंल उपभोग ने मनुष्य को संवेदनहीन और विवेकशून्य व्यक्ति में तब्दील कर दिया
है। जिससे मनुष्यता अवमूल्यित हो रही है, नैतिकता का ह्रास
हो रहा है। ऐसे समय में विमलेश त्रिपाठी अपनी कलम और अपनी आस्था के सहारे मनुष्य
की जिन्दादिली और जज्बात को बचाने की जद्दोजहद करते हैं। वे नाउम्मीद नहीं होते।
पिछले दिनों अन्ना आंदोलन, निर्भया आंदोलन तथा आम आदमी
पार्टी को मिला अपार समर्थन तथा जनता की सक्रिय भागीदारी हम सबकी उम्मीद को बल
देती है। ‘अभिव्यक्ति के खतरे’ उठाकर
विमलेश त्रिपाठी मृतात्माओं के गढ़ और मठ ध्वस्त करने की दिशा में सक्रिय होते
हैं। इस मुश्किल दौर में कविता एकमात्रा ऐसा साधन है जिस पर भरोसा किया जा सकता
है। वह एक ऐसे मंत्रा की तरह है जो मृतात्माओं में प्राणों का संचार कर सकती है।
इसीलिए कवि विमलेश त्रिपाठी इस उम्मीद को थामते हैं और रचनात्मक संकल्प के साथ
परिवर्तन और प्रतिरोध की दिशा में सक्रिय होते हैं। उनका कवि और उसकी कविताई में
गहरा यकीन है। वे लिखते हैं –
‘‘लेकिन हर देश में और हर समय में जिन्दा रहती हैं कुछ
विलुप्त मान ली गई प्रजातियाँ
वे छुप-छुपकर रहती हैं जिन्दा और कुछ के पास तो जन्मतः
ही होता है एक कवच-कुण्डल और
जिन्हें मार पाना कभी भी नहीं रहा आसान किसी भी तंत्र के
लिए।’’
और ऐसे लोग ‘वेश बदलकर फैल गए पूरे देश में शब्दों के जादू मंतर लेकर जिन्दा करने मरे
हुए लोगों को’। अन्ततः मृत लोगों में प्राणों का संचार होता
है और ‘लोग जुटते गए और कारवाँ बनता गया’ की तर्ज पर वे अन्ततः मृत राजा को पदच्युत कर देते हैं। लेकिन कवि उस
मनुष्य-संहारक मशीन को अर्थात् अनवरत आपाधपी की कोल्हू के बैल जैसी जिन्दगी देने
वाली व्यवस्था को नष्ट करके एक संतुलित और मानवीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहता
है। मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और धूमिल आदि कवियों के रचनात्मक
मुहावरे में लिखी गयीं उनकी कविताएं अपने गठन में बिखराव के बावजूद महत्वपूर्ण
कविताएं बन पड़ी हैं। कवि के मानस में उमड़ती-घुमड़ती अनेक चिंताएं और सवाल कविता
में ढलने को विकल हैं, इसलिए कहीं-कहीं उनकी अभिव्यक्ति में
बिखराव आ गया है। यत्र-तत्र आवेग और आक्रोश की कमी के चलते आई थोड़ी शिथिलता और
ठण्डेपन से भी उनकी कविताओं की सम्प्रेषणीयता बाधित होती है।
–– रसाल सिंह
किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली-07
फोन: 8800886847
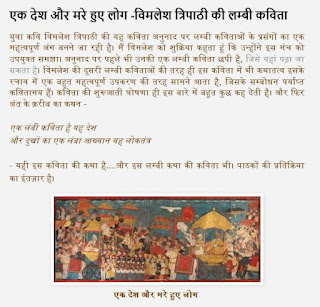
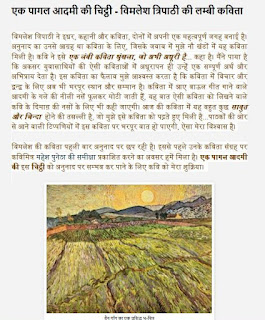
बहुत सटीक विवेचना