‘मदर इंडिया’ और ‘हम मांस के थरथराते झंडे हैं’
ये हमारे समय के
दो महत्वपूर्ण युवा कवि और उनकी कविताएं हैं। कवियों ने इन्हें अलग-अलग
समयों, स्थानों और तनाव में सम्भव
किया है। गीत की कविता को भारतभूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला, इसलिए
वह बहुपठित कविता है। अंशु की कविता उतनी नहीं पढ़ी गई है।
मैं दोनों कविताओं को यहां एक साथ एक पृष्ठ पर लेकर कविता के इलाक़े में उपस्थित
एक प्रिय-आत्मीय साम्यवाद और उससे अपने लगाव को रेखांकित कर रहा हूं। इसके पहले
मैंने इसी समझ के साथ व्योमेश शुक्ल और सिद्धान्तमोहन तिवारी की कहरवा पर लिखी दो कविताओं को साथ लगाया था।
कवि आपस में उतना संवाद कायम नहीं कर
पाते….अकसर आपस में मिल भी नहीं पाते…पर उनकी कविता उन्हें अचानक किसी मोड़
पर मिला देती है तो ऐसे दृश्य सम्भव होते हैं, जिसे उनके
बीच एक अनहुए संवाद की तरह देखा और पढ़ा जा सकता है।
गीत मेरा ऐसा कविमित्र है, जिससे अकसर इंटरनेट पर और कभी-कभी फोन पर भी संवाद हो जाता है…एक-दूसरे के हालचाल लेते हैं और वक़्त हुआ तो कुछ देर अपनी लिखत-पढ़त के बारे में बतियाते हैं…इस तरह हम निकट हैं…रहेंगे। अंशु से न मैं कभी मिला और न बात हुई। उसका संग्रह दक्खिन टोला नैनीताल में काफी पहले हुए एक पुस्तक मेले में लालबहादुर वर्मा जी ने भेंट दिया था…तब से अंशु भी साथ है…निकट है…रहेगा।
***
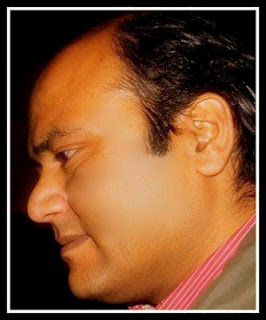 |
| गीत चतुर्वेदी |
मदर इंडिया – गीत चतुर्वेदी
(उन दो
औरतों के लिए, जिन्होंने कुछ दिनों तक शहर को डुबो दिया था)
दरवाज़ा खोलते ही झुलस जाएं आप शर्म की गर्मास से
खड़े-खड़े ही गड़ जाएं महीतल, उससे भी नीचे रसातल तक
फोड़ लें अपनी आंखें निकाल फेंके उस नालायक़ दृष्टि को
जो बेहयाई के नक्की अंधकार में उलझ-उलझ जाती है
या चुपचाप भीतर से ले आई जाए
कबाट के किसी कोने में फंसी इसी दिन का इंतज़ार करती
किसी पुरानी साबुत साड़ी को जिसे भाभी बहन मां या पत्नी ने
पहनने से नकार दिया हो
और उन्हें दी जाएं जो खड़ी हैं दरवाज़े पर
मांस का वीभत्स लोथड़ा सालिम बिना किसी वस्त्र के
अपनी निर्लज्जता में सकुचाईं
जिन्हें भाभी मां बहन या पत्नी मानने से नकार दिया गया हो
कौन हैं ये दो औरतें जो बग़ल में कोई पोटली दबा बहुधा निर्वस्त्र
भटकती हैं शहर की सड़क पर बाहोश
मुरदार मन से खींचती हैं हमारे समय का चीर
और पूरी जमात को शर्म की आंजुर में डुबो देती हैं
ये चलती हैं सड़क पर तो वे लड़के क्यों नहीं बजाते सीटी
जिनके लिए अभिनेत्रियों को यौवन गदराया है
महिलाएं क्यों ज़मीन फोड़ने लगती हैं
लगातार गालियां देते दुकानदार काउंटर के नीचे झुक कुछ ढूंढ़ने लगते हैं
और वह कौन होता है जो कलेजा ग़र्क़ कर देने वाले इस दलदल पर चल
फिर उन्हें ओढ़ा आता है कोई चादर परदा या दुपट्टे का टुकड़ा
ये पूरी तरह खुली हैं खुलेपन का स्वागत करते वक़्त में
ये उम्र में इतनी कम भी नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं
ये कौन-सी महिलाएं हैं जिनके लिए गहना नहीं हया
ये हम कैसे दोगले हैं जो नहीं जुटा पाए इनके लिए तीन गज़ कपड़ा
ये पहनने को मांगती हैं पहना दो तो उतार फेंकती हैं
कैसा मूडी कि़स्म का है इनका मेटाफिजिक्स
इन्हें कोई वास्ता नहीं कपड़ों से
फिर क्यों अचानक किसी के दरवाज़े को कर देती हैं पानी-पानी
ये कहां खोल आती हैं अपनी अंगिया-चनिया
इन्हें कम पड़ता है जो मिलता है
जो मिलता है कम क्यों होता है
लाज का व्यवसाय है मन मैल का मंदिर
इन्हें सड़क पर चलने से रोक दिया जाए
नेहरू चौक पर खड़ा कर दाग़ दिया जाए
पुलिस में दे दें या चकले में पर शहर की सड़क को साफ़ किया जाए
ये स्त्रियां हैं हमारे अंदर की जिनके लिए जगह नहीं बची अंदर
ये इम्तिहान हैं हममें बची हुई शर्म का
ये मदर इंडिया हैं सही नाप लेने वाले दर्जी़ की तलाश में
कौन हैं ये
पता किया जाए.
दरवाज़ा खोलते ही झुलस जाएं आप शर्म की गर्मास से
खड़े-खड़े ही गड़ जाएं महीतल, उससे भी नीचे रसातल तक
फोड़ लें अपनी आंखें निकाल फेंके उस नालायक़ दृष्टि को
जो बेहयाई के नक्की अंधकार में उलझ-उलझ जाती है
या चुपचाप भीतर से ले आई जाए
कबाट के किसी कोने में फंसी इसी दिन का इंतज़ार करती
किसी पुरानी साबुत साड़ी को जिसे भाभी बहन मां या पत्नी ने
पहनने से नकार दिया हो
और उन्हें दी जाएं जो खड़ी हैं दरवाज़े पर
मांस का वीभत्स लोथड़ा सालिम बिना किसी वस्त्र के
अपनी निर्लज्जता में सकुचाईं
जिन्हें भाभी मां बहन या पत्नी मानने से नकार दिया गया हो
कौन हैं ये दो औरतें जो बग़ल में कोई पोटली दबा बहुधा निर्वस्त्र
भटकती हैं शहर की सड़क पर बाहोश
मुरदार मन से खींचती हैं हमारे समय का चीर
और पूरी जमात को शर्म की आंजुर में डुबो देती हैं
ये चलती हैं सड़क पर तो वे लड़के क्यों नहीं बजाते सीटी
जिनके लिए अभिनेत्रियों को यौवन गदराया है
महिलाएं क्यों ज़मीन फोड़ने लगती हैं
लगातार गालियां देते दुकानदार काउंटर के नीचे झुक कुछ ढूंढ़ने लगते हैं
और वह कौन होता है जो कलेजा ग़र्क़ कर देने वाले इस दलदल पर चल
फिर उन्हें ओढ़ा आता है कोई चादर परदा या दुपट्टे का टुकड़ा
ये पूरी तरह खुली हैं खुलेपन का स्वागत करते वक़्त में
ये उम्र में इतनी कम भी नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं
ये कौन-सी महिलाएं हैं जिनके लिए गहना नहीं हया
ये हम कैसे दोगले हैं जो नहीं जुटा पाए इनके लिए तीन गज़ कपड़ा
ये पहनने को मांगती हैं पहना दो तो उतार फेंकती हैं
कैसा मूडी कि़स्म का है इनका मेटाफिजिक्स
इन्हें कोई वास्ता नहीं कपड़ों से
फिर क्यों अचानक किसी के दरवाज़े को कर देती हैं पानी-पानी
ये कहां खोल आती हैं अपनी अंगिया-चनिया
इन्हें कम पड़ता है जो मिलता है
जो मिलता है कम क्यों होता है
लाज का व्यवसाय है मन मैल का मंदिर
इन्हें सड़क पर चलने से रोक दिया जाए
नेहरू चौक पर खड़ा कर दाग़ दिया जाए
पुलिस में दे दें या चकले में पर शहर की सड़क को साफ़ किया जाए
ये स्त्रियां हैं हमारे अंदर की जिनके लिए जगह नहीं बची अंदर
ये इम्तिहान हैं हममें बची हुई शर्म का
ये मदर इंडिया हैं सही नाप लेने वाले दर्जी़ की तलाश में
कौन हैं ये
पता किया जाए.
***
मदर इंडिया के बारे में गीत का कथन –
(इस कविता में जो घटना आती है, वह मेरे शहर मुंबई के पास स्थित उपनगर उल्हासनगर की है. एक दिन ये दोनों औरतें हमारे दरवाज़े पर आ खड़ी हुई थीं. बात 1995 की रही होगी. 1996 से 2001 तक मैंने लगातार कविताएं लिखीं. फिर ब्रेक लग गया. लंबा. 2001 में ही भास्कर ज्वाइन किया और तब से कई शहरों में डेरे डाले. 2005 में भोपाल पहुंचा, तो वहां कुमार अंबुज ने बहुत प्रेरित किया लिखने को. मदर इंडिया उस पारी की पहली कविता थी. वागर्थ ने अक्टूबर 2006 अंक में छापा इसे. और मई 2007 में इस पर भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार की घोषणा हुई.)
****
 |
| अंशु मालवीय |
हम मांस के थरथराते झंडे हैं – अंशु मालवीय
देखो हमें
हम मांस के थरथराते झंडे हैं
देखो बीच चौराहे पर बरहना हैं हमारी वही छातियाँ
जिनके बीच
तिरंगा गाड़ देना चाहते थे तुम
देखो सरेराह उघडी हुई
ये वही जांघे हैं
जिन पर संगीनों से
अपनी मर्दानगी का राष्ट्रगीत
लिखते आए हो तुम
हम निकल आयें हैं
यूं ही सड़क पर
जैसे बूटों से कुचली हुई
मणिपुर की क्षुब्ध लरजती धरती
अपने राष्ट्र से कहो घूरे हमें
अपनी राजनीति से कहो हमारा बलात्कार करे
अपनी सभ्यता से कहो
हमारा सिर कुचल कर जंगल में फैंक दे हमें
अपनी फौज़ से कहो
हमारी छोटी उंगलियाँ काटकर
स्टार की जगह लगा ले वर्दी पर
हम मांस के थरथराते झंडे हैं
देखो बीच चौराहे पर बरहना हैं हमारी वही छातियाँ
जिनके बीच
तिरंगा गाड़ देना चाहते थे तुम
देखो सरेराह उघडी हुई
ये वही जांघे हैं
जिन पर संगीनों से
अपनी मर्दानगी का राष्ट्रगीत
लिखते आए हो तुम
हम निकल आयें हैं
यूं ही सड़क पर
जैसे बूटों से कुचली हुई
मणिपुर की क्षुब्ध लरजती धरती
अपने राष्ट्र से कहो घूरे हमें
अपनी राजनीति से कहो हमारा बलात्कार करे
अपनी सभ्यता से कहो
हमारा सिर कुचल कर जंगल में फैंक दे हमें
अपनी फौज़ से कहो
हमारी छोटी उंगलियाँ काटकर
स्टार की जगह लगा ले वर्दी पर
हम नंगी निकल आयीं हैं सड़क पर
अपने सवालों की तरह नंगी
हम नंगी निकल आयीं हैं सड़क पर
जैसे कड़कती है बिजली आसमान में
बिल्कुल नंगी…….
हम मांस के थरथराते झंडे हैं
अपने सवालों की तरह नंगी
हम नंगी निकल आयीं हैं सड़क पर
जैसे कड़कती है बिजली आसमान में
बिल्कुल नंगी…….
हम मांस के थरथराते झंडे हैं
***
(मणिपुर-जुलाई 2004, सेना ने मनोरमा नाम की महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। मनोरमा के लिए न्याय की मांग करती महिलाओं ने निर्वस्त्र हो प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन की हिस्सेदारी के लिए यह कविता।)
****
ईद की मुबारकबाद
बहुत ही सुन्दर और मार्मिक भावपूर्ण रचनाओं का संकलन … वाह वाह
????
बहुत सुन्दर चयन . यह चयन खुद ही कविता के बारे कुछ कह्ता है. अच्छी कविता की एक खासियत यह भी मानी गई है कि वह और अच्छी कविता कहने के लिए उकसाती है . दो औरतों वाली कविता ऐसी ही है. औरत के ये बिम्ब बहुत कॉमन हैं अपने देश में . फलतः कविता मे भी .पहली कविता मुझे 'तोड़ती पत्थर' याद आती है. उस की बाद अलग अलग रूप मे यह ताक़तवर औरत हिन्दी कविता मे आती ही रही है. लेकिन हर बार ये बिम्ब हमें थोड़ा और हिला देते हैं . थोड़ा और ज़िन्दा कर देते हैं . और हर बार हम कुछ और कहने , जोड़ने के लिए व्याकुल हो जाते हैं ……….
दूसरी कविता एक अनकॉमन ईवेंट से प्रेरित है . यह ईवेंट सन्न कर देने वाला था. हमारे देश की सामान्य प्रवृत्ति के अनुकूल नही था , और शायद इसी वजह से सोच की एक नई खिड़की खोलने वाला था . हम एक दम इस मे कुछ जोड़ नही सकते . हमे मज़बूरन चुप होना पड़ता है इस कविता को पढ़ कर . क्यों ? क्यों कि यह नई आवाज़ है . हाशिये की आवाज़ . हमारी हिन्दी कविता ने बहुत देरी से ये आवाज़ें दर्ज करनी शुरू की हैं . यह कविता इस बात का पता देती है कि हाशिए मे क्या चल रहा है. क्या मानसिकता पनप रही है ? यह कविता इरोम शर्मिला की याद दिलाती है, जो खुद इस नई आवाज़ का प्रतीक है. यह कविता अभी अभी असम की एक शर्मनाक घटना की याद दिलाती है. हम इन आवाज़ों का क्या करें ? हमे इन आवाज़ों की पहचान के लिए मशक्कत करने की ज़रूरत नही महसूस होती . हम जानते हैं ये आवाज़ें कौन हैं . लेकिन हम ने कभी इन आवाज़ों को अपना समझा ही नहीं शायद .
मैं गीत की आज की कविताओं में इस पुरानी धुन को ढूंढता हूँ और उदास होता हूँ…
और अंशु की लम्बी चुप्पी देखता हूँ और उदास होता हूँ.
मैं इन उदासियों को एक दिन उदास होते देखना चाहता हूँ.
Amazing to read..thought provoking..
इन दोनों मन के सबसे निचली तल तक कुरेद देने वाली कविताओं के रचयिताओं को …साथ साथ पाठकों तक इन्हें पहुँचाने वाले साथी को भी … सम्मान पूर्वक गले से लगा लिया जाना लाजिमी है…यहाँ शुक्रिया शब्द बिलकुल ही नाकाफी होगा.समाज की इन कुरूप पर बगावती करवटों को आम तौर पर किताबों में जगह नहीं मिलती पर कहीं न कहीं लेखक कवि अपनी चौकस निगाहों से उनके आवेग को पकड़ ही लेता है और जन इतिहास के हवाले कर देता है.प्रतिकार के अबतक आजमाए हथियार जब भोथरे हो गये तो हमारी नयी पीढ़ी इन्हीं तेज धार हथियारों की ओर देखेगी…रामदेव और अन्ना हजारे के नाकाम आंदोलनों के बरक्स इनकी ताकत समय जरुर तोलेगा….
यादवेन्द्र
सुन्दर कवितायेँ ….
गीत की कविता तो पहले भी पढ़ी है.. पुरस्कृत कविता है … इसलिए ज्यादा पढ़ी गयी है (ये आपने भी रेखांकित किया है) पर अंशु की कविता का फलक बहुत बड़ा और व्यापक है ..साथ ही उसकी पीड़ा भी बेहद सान्द्र है…