कविता जो साथ रहती है / 2 – विनोद कुमार शुक्ल की कविता : गिरिराज किराड़ू
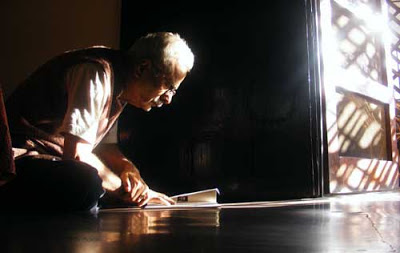 |
| कवि की तस्वीर रविवार से साभार |
गिरिराज किराड़ू ने अपने स्तम्भ की दूसरी कविता के रूप में विनोद कुमार शुक्ल की कविता का चयन किया है, जो संयोग से मेरी भी प्रिय कविता रही है। गिरिराज की ये टिप्पणियां किसी भी औपचारिक अनुशासन के बाहर बहुत भरे दिल की पुकार हैं। ‘पहले से अधिक विभाजित और अन्यायी ग्रह पर मरने’ की त्रासदी हम सबकी है, इसलिए यह पुकार भी उम्र भर के लिए हमारे दिल में घर कर जाएगी। नवीन सागर पर इस स्तम्भ की पहली टिप्पणी हमारे पाठक यहां पढ़ सकते हैं।
***
जो मेरे घर कभी नहीं आएँगे
जो मेरे घर कभी नहीं आएँगे
मैं उनसे मिलने
उनके पास चला जाऊँगा।
एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर
नदी जैसे लोगों से मिलने
नदी किनारे जाऊँगा
कुछ तैरूँगा और डूब जाऊँगा
पहाड़,
टीले,
चट्टानें,
तालाब
असंख्य पेड़ खेत
कभी नहीं आयेंगे मेरे घर
खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने
गाँव-गाँव,
जंगल-गलियाँ जाऊँगा।
जो लगातार काम से लगे हैं
मैं फुरसत से नहीं
उनसे एक जरूरी काम की तरह
मिलता रहूँगा –
इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह
सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा।
सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा।
इस
कविता के पहले वाक्य ने जो तीन छोटी काव्य पंक्तियों में फैला है ने पढ़ते ही बाँध
लिया था. मैं जिस तरह के समाज में, पड़ोस और मोहल्ले के जिस घेराव में बड़ा हुआ था
उसमें वे लोग जो मेरे घर कभी नहीं आयेंगे वे अक्सर ‘बाहर’ के लोग नहीं थे, वे लोग थे जिनसे कभी प्यार रहा होगा, जिनसे अब
रंजिश है (अंतरंग शत्रु, इंटिमेट एनिमी?) और इस लिए वे मेरे घर नहीं आयेंगे मैं
उनके घर नहीं जाऊंगा. कुछ ऐसा अपने में गाफिल संसार था छोटा-सा. ‘नाली साफ़ करने
वाली के हाथ नहीं लगाना है’ से ‘बाहरी’ का अनुभव उस तरह से शुरू नहीं हुआ था; ‘आउटसाइडर’ की कल्पना के लिए जगह बहुत बाद में
बनी जब परकोटे के भीतर के ही ‘मुसलमान’ और परकोटे के बाहर के “यूपी
वाले……” और “….. बिहारी” पान की दुकानों और निठल्ली दोपहरों
के किस्सों में आये.
और उसके बाद तो ‘बाहर’ बहुत बड़ा होता गया, जितना भूगोल में नहीं उससे ज्यादा अपने भीतर और लगा यह पृथ्वी ऐसे लोगों से भरी है जो मेरे घर कभी नहीं आयेंगे और रंजिश अक्सर कोई वजह नहीं होगी उसकी. बल्कि वे जो मेरे घर आयेंगे वह एक बहुत छोटी-सी, छटांक-भर जनसँख्या ही रहेगी और अब उसे पूरा संसार समझने जितना गाफिल रहना मुश्किल होता जा रहा है. मैं असंख्य लोगों के घर गये बिना और असंख्य लोग मेरे घर आये बिना मर जायेंगे. यह सब बहुत अस्पष्ट तरीके से मन में चलता रहा था जब यह कविता जीवन में आयी. और तुरंत तो इसके ‘समाधान’ ने बाँध लिया. जो मेरे घर कभी नहीं आयेंगे उन लोगों से मिलने जाना ही इस समस्या का समाधान है.
लेकिन तीन छोटी काव्य पंक्तियों से आगे बढते ही कविता मनुष्यों की नहीं उफनती नदी, पहाड़, टीले, चट्टानें, तालाब असंख्य पेड़ खेत की बात करती है जो इस कविता के वाचक के घर कभी नहीं आयेंगे और अंत में उनकी भी जो लगातार काम से लगे हैं. क्या यह वाचक कभी उन सबके – नदी जैसे लोगों के, खेत खलिहानों जैसे लोगों के – घर जा पायेगा? या यह उसकी सद्कामना भर है? अकर्मक सद्कामना! यह पद – अकर्मक सद्कामना – बाद में बहुत परेशान करने वाला रहा है. कई अरब लोगों से मिल पाना तो किसी भी तरह संभव नहीं फिर यह कविता इतना सटीक लेकिन असंभव समाधान क्यूँ पेश करती है? सद्कामना कर्म की एवजी क्यूँ है? इसलिए नहीं कि वह कर्म-आतुर नहीं बल्कि इसलिए कि उसे इस कर्म की असंभाव्यता का ठीक ठीक अंदाज़ है? वह एक असंभव कर्म की कामना इसीलिये करती है कि केवल कामना में, कविता में ही असंभव को भी इस तरह ‘किया’ जा सकता है?
2
विनोद
कुमार शुक्ल की कविता में प्रकृत और आदिवास अभिलेख नहीं हैं. वे एक खोयी हुई
दुनिया नहीं है जिसकी और ‘लौटना’ होगा – एक पुकार जो कभी योरोपीय रोमेन्टिसिज्म
में सुनाई दी थी. और जिसकी परिणति, ऐसा कई अध्ययन कहते हैं, जर्मन नाजीवाद में हुई
थी. विनोद कुमार शुक्ल के लेखन में लौटने
की जगह है : घर. प्रकृत और आदिवास नहीं, घर वह जगह जहाँ वह लौटते हैं. बार बार.
प्रकृत और आदिवास के पास जाना है , लौटना नहीं है.
3
एक साक्षात्कार में आलोक पुतुल ने विनोदजी को सीधे पूछा है कि क्यूँ बहुत कुछ उनके लेखन में केवल सद्कामना है? इसी कविता में कर्म नहीं कर्म की कामना है. कर्म और कामना के बीच नैतिक हायरार्की में कामना सदैव निम्नतर क्यूँ? कला में सद्कामना एक बनावट से अधिक कैसे बनती है? कला अपने में कर्म है या उसमें से जो झांकता है वही कर्म हो सकता है, और वह भी हमेशा नहीं, जैसे इस कविता में नहीं?
हर कविता दो बार एक कर्म है : एक बार जब वह लिखी जाती है, दूसरी बार जब वह पढ़ी जाती है. और यह दूसरा कर्म कई कई बार होता है. इतनी बार जो कर्म है उसकी अंतर्वस्तु सद्कामना है? क्या हर पठन में इसकी अंतर्वस्तु वैसी ही बनी रहती है? क्या हर बार एक सद्कामना ही पाठकर्ता का हासिल होती है? या कविता की सद्कामना एक पाठकर्ता के लिए कर्म या उसकी उत्प्रेरणा बन सकती है? इस कविता का हर पाठक क्या यह कामना भर करेगा कि वह सबके घर जायेगा या वह कुछेक के घर ‘सचमुच’ जायेगा भी? क्या कुछ गये भी? इन पाठकर्ताओं में स्वयं लेखक भी शामिल है. खुद उसके लिए यह कविता क्या किसी कर्म की उत्प्रेरणा बन पाई?
पर विनोदजी से ऐसा प्रश्न पूछने के लिए आपका नाम आलोक पुतुल होना चाहिए.
4
फुरसत चिढ़ाने वाला शब्द है.
फुरसत
समर्थ का विकल्प है.
फुरसत
एक जरूरी काम है अगर आपको सबके घर जाना है.
5
अब जबकि दूसरों के घर और मन तक जाने के गोरखधंधे में दिल पर कई खरोंचें भी लग चुकी हैं (मेरी तो मैं कह ही रहा हूँ, दूसरों के जो मैंने लगाई होंगी वे भी), अब जबकि दूसरों के घर और मन तक जाने का इरादा पहले जितना निश्चय भरा तो कतई नहीं है, अब जबकि सद्कामना और सकर्मकता का भेद अपनी विज्ञापित जटिलता तज कर अपनी सहज सरलता की ओर बढ़ रहा है मेरे लिए, तो यह कविता हर दूसरे दिन याद आती है.
अब जबकि बाहर इतना है कि उसके पहले जो था मेरे पास वह अर्थहीन हो जा रहा है , अब जबकि घर कहने से आने वाली यादों में दश्त की याद भी शामिल हो गयी है, अब जबकि मैं एक दूसरा हूँ यह कविता अपने और पराये, घर और बाहर, सद्कामना और सकर्मकता को एक दोहे-सा बांधती हुई बार बार हर दूसरे आँसू याद आती है – मैं कर्म की अपनी मामूली कोशिशों के साथ सद्कामना के अरण्य में किसी दीदा-ए-तर की अनुकृति होने की कोशिश में पहले से अधिक विभाजित और अन्यायी ग्रह पर ही मरूंगा? न्याय बस का नहीं था, अन्यायी जद में नहीं था लेकिन जितने लोगों के घर जा सकते थे, जितनों को अपने ‘यहाँ’ बुला सकते थे उसका एक ज़रा सा हिस्सा भी नहीं किया, और इसे अपनी पहली या अकेली नहीं, बस आखिरी इच्छा की तरह लेते हुए ही जायेंगे?
***
यह अनुनाद की 583वीं पोस्ट है
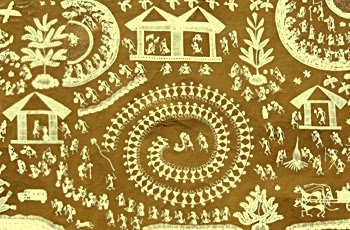

अाखिरी पैरा अाप में किसी काविता की तरह है, पढवाने के लिये धन्यवााद!
गिरिराज भाई, यह समीक्षा कविता के पाठ की वृहत्तर परिधि के बाहर चली जाती है. कविता की 'लोकेशन' हमेशा कर्म ही रहे हैं. शुक्ल जी को याद करिए, लोकमंगल की साधनावस्था हमेशा सिद्धावस्था से बेहतर कविता की भूमि बनती है.
मृत्युंजय: इस लिखे में कोई समीक्षा तत्व आ भले गया हो, यह लिखा समीक्षा की तरह नहीं गया है। यह स्तम्भ ऐसे सोचा नहीं गया है। कविता की लोकेशन 'कर्म' होते हैं, लेकिन हर कवि को अपने ढंग से कोशिश करना पड़ती है।
स्वप्नदर्शी: शुक्रिया।
वही जानी-पहचानी काव्याभासी लफ्फाजी! प्रतिरोध की जहाँ संभावना भी उपजे वहां शब्दजाल के बीच कायरता और अकर्मक सदिच्छा का कुहासा फैला देना…माफ़ करिये शिरीष महोदय इसके लिए अनुनाद का उपयोग करने की अनुमति दे आप भी इसके हिस्सा बन रहे हैं. (इसे चाहें तो बस पढ़ के मिटा दें..एक शुभेच्छु हूँ बुरा नहीं मानूंगा)
आप अपना नाम दे सकें तो आभारी रहूंगा भाई …..
गिरिराज …जब आपने कविता की टिपण्णी का शीर्षक "सद्कामना के अरण्य "में लिखा तब ही समझ आता है की आप कविता में कवि के उस भाव को जो निर्मल और पवित्र व् बहुत ही सहज रूप से आया है ….उस भाव के लिए इस कविता को पसंद करते है और उसके लिए कुछ लिखना पसंद करते है …."मैं फुर्सत से नहीं एक जरुरी काम की तरह मिलता रहूँगा ."……कवि अरण्य में जाता है ….अरण्य की सम्पदा से आकर्षित नहीं होकर वहा से कुछ लेने नहीं वरन देने की बात करने …ये अनोखा व् नया भाव इस कविता की शक्ति है …और आपने इस सुक्ष्म भाव को पकड़ा …बधाई …भाई बहुतअच्छा लिख लेते हो …वाह …शाबाश ….जीते रहो !!!