दिविक रमेश की कविताएं
चाहता हूं किसी अवतार की तरह
में क्रूरतम बलात्कार की शिकार दामिनी के पक्ष में २१-१२-२०१२ को उमड़े जन सैलाब को
देखकर)
नहीं कह सकता इसे!
हैं ये रेलगाड़ियों पर होकर काबिज ।
में ढर्रेदार झंडे भी तो नहीं हैं
देखने के आदी हैं हम। खासकर जन्तर-मन्तर और इंडिया गॆट पर।
नेता तक लापता हैं दूर दूर तक
यह जहां भाषण से अधिक लावा उमड़ रहा है हर ओर से!
बंदोबस्त ज़रूर वैसा ही है जैसा होता आया है अक्सर।
गया है पूरा राजपथ जन सैलाब से
गया हो जैसे जनपथ में
ही कहना ठीक रहेगा इसे।
कविताओ,
कर लो दर्ज इसे
न दिया जाए
इतिहास रच रहा यह दृश्य।
सोचता हूं उतनी ही पड़ रही हैं माथे पर चिन्ता की रेखाएं
अधूरी पड़ रही हैं संज्ञाएं
स्वयंभू जन सैलाब कहना उचित हो अधिक।
लग रहा कि जैसे निकल आई हों हाथों में लिए मशालें
निकालती तमाम कविताएं ’चांद का मुह टेढ़ा है” की
हों सड़क से संसद तक
ही पड़ी थी अब तक।
कोहरे से कैसे निकल आईं हैं ये पंक्तियां
बार
कर देखो
जाएगा।’
हूं
किस धारा में बांध कर देखूं इसे
से मुक्त स्वयंभू जन सैलाब को!
है यह
दूर दूर तक लग गया हो कर्फ्यू धर्म की दुकानों पर
रसातल में भी नहीं जगह
खुजलाने तक का नहीं अवसर जहां मानो जातियों को राहत में!
है यह
प्रतीक्षा में जाने कब से खप रही थीं भयभीत, दुबकी बेऔक़ात कर
दी गईं
की आंखें
जो बुझी लालटेनों सी अपने कोटरों पर।
तो नहीं है यह
प्रतीक्षा में सूख कर दरकने लगी थी उम्मीदों की पृथ्वी
तो नहीं है यह
प्रतीक्षा में खड़ा होता गया था ’क्या फर्क पड़ता है’ जैसे उदास मुहावरों का
तो नहीं है यह
प्रतीक्षा में कविताएं तक छिपने लगी थीं शंकाओं और प्रश्नों के आवरणों में।
राजनीतियां!
यह
मेरी आस्थाओं की लाशों में सांसें।
यह
पूजना चाहता हूं इसे किसी अवतार की तरह।
माँ गाँव में है
चाहता था
आ बसे माँ भी
यहाँ, इस शहर में।
पर माँ चाहती थी
आए गाँव भी थोड़ा साथ में
जो न शहर को मंजूर था न मुझे ही।
न आ सका गाँव
न आ सकी माँ ही
शहर में।
और गाँव
मैं क्या करता जाकर!
पर देखता हूँ
कुछ गाँव तो आज भी ज़रूर है
देह के किसी भीतरी भाग में
इधर उधर छिटका, थोड़ा थोड़ा चिपका।
माँ आती
बिना किए घोषणा
तो थोड़ा बहुत ही सही
गाँव तो आता ही न
शहर में।
पर कैसे आता वह खुला खुला दालान, आंगन
जहाँ बैठ चारपाई पर
माँ बतियाती है
भीत के उस ओर खड़ी चाची से, बहुओं
से।
करवाती है मालिश
पड़ोस की रामवती से।
सुस्ता लेती हैं जहाँ
धूप का सबसे खूबसूरत रूप ओढ़कर
किसी लोक गीत की ओट में।
आने को तो
कहाँ आ पाती हैं वे चर्चाएँ भी
जिनमें आज भी मौजूद हैं खेत, पैर,
कुएँ और धान्ने।
बावजूद कट जाने के कालोनियाँ
खड़ी हैं जो कतार में अगले चुनाव की
नियमित होने को।
और वे तमाम पेड़ भी
जिनके पास
आज भी इतिहास है
अपनी छायाओं के।
दैत्य ने कहा
दैत्य ने कहा मैं घोषणा करता हूं
कि आज से सब स्वतंत्र हैं
कि सब ले सकते हैं आज से
भुनते हुए गोश्त की लाजवाब महक।
सब ख़ुश हुए क्योंकि सब को ख़ुश होना चाहिए था।
कितना उदार है दैत्य
दैत्य ने कहा
तकाजा है नैतिकता का कि नहीं भूनने चाहिए हमें दूसरों के शरीर
वह भी महज भुनते हुए गोश्त की महक के लिए।
सबने स्वीकार किया।
कितना महान है दैत्य
दैत्य ने कहा
खुद को जलाकर खुद की महक लेना
कहीं बेहतर कहीं पवित्र होता है महक के लिए।
सबने माना और झोंक दिया आग में खुद को।
कितना इंसान है दैत्य
दैत्य ने कहा
तुम्हें गर्व होना चाहिए खुद की कुर्बानियों पर
सब और और भुनने लगे मारे गर्व के।
कितना भगवान है दैत्य
दैत्य ने कहा
पर इस बार खुद से
कितना लाजवाब होगा इन मूर्खों का महकता गोश्त
आज दावत होगी दैत्यों की।
दैत्य हंसता रहा हंसता रहा
झरता लावा
नहीं छोड़ती
माँ-बहिन को भी
कहावत
छोड़ते कई
को भी ।
की तरह
जाता है सब जायज
जाता है शान्त ।
हाहाकार भी
।
कवायद है
झरता रहता है लावा
पड़ता है
पसीने की आग को
पड़ता है
गलियारों में
ढंडी आहों को ।
स्वीकृति है
होने लगती है नपुंसकता
विशेष में
दिए गए एक खास प्रधानमंत्री की ।
होने लगती हैं
विरोधियों की शिखण्डी हरकतें भी ।
के इस देश में
मजबूर हैं
वारांगनाओं सी
हैं तालियाँ- वाम भी अवाम भी ।
होते हैं सब नंगे-
पराए भी ।
निरर्थकता
की,
नदियों की
रहा है मन
बची
पड़ी नहरों में
।
लौ-सी जलती
बर्फों में ।
अध्यात्म तो नहीं हो रहा हूं मैं !
अध्यात्म
जाग जाएं पत्ते वृक्षों के ।
अगर निरपेक्ष पड़ी वनस्पतियाँ ।
अगर बांसों में सुप्त नाद ।
सके भरोसा अस्पताल अपनी राहों में
का ।
तो हो सकती है
जंगल और बियाबान भी।
होते हैं तालियों के बियाबान
नीचे आ जाया करते हैं
गड़गड़ाहट से आसमान।
होता है
होता है
अर्थ तालियों की
होती आवाज़ का।
मैंने एक ऎसा भी हलका
होता था
अर्थ लगाना।
मेरी मां की हथेलियों का
हथेलियों का
हैं रोटियां
की थाप से।
के बीच रख लोई
मां
आकार
की आवाज में ।
होती है आवाज थाप की।
होती है
नहीं होती।
थी तो मां
आकार आज भी रोटियों को
की थाप से।
समझ पाता है कोई अर्थ
ज्यादा आवाज का।
रह जाती है आवाज
उपेक्षित रह जाती थी मां
आकार आज भी रोटियों को
की थाप से।
आवाज आकार लेती रोटियां
पाती है आवाज
साथ-साथ
बदलती हुई रोटी में
एक लय
तवे में,
में,
तवे में
थाली में।
है
की क्यों न हो,
खामोश ।
सकती है
उनका दर्द-मेरी जुबान
हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी
शायद वह आतंकवादी भी नहीं है
जो भून डालता है महज भूनने के लिए
जिसके पास है भी कोई समझ या दॄष्टि –
संदेह ही बना रहता है ।
हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी
शायद यह है
कि हमारे ही सामने, हमारे ही मुहल्लों
में
हमारी ही समझ की छतों के नीचे
हमारे दर्दों को भी हमारा नहीं रहने दिया जाता ।
बस छीन लिया जात है हमसे –
न कोई कीमत, न कोई मुआवजा !
कैसी त्रासदी है न
होते ही उनका
हमारा दर्द हमें ही पहचानने से इंकार कर देता है –
ओपरा ओपरा होकर आंखें चुराता है
।
बड़े घर के कुत्तों-सा लगता है घूमने बड़ी बड़ी गाड़ियों में ।
कहां-कहां तक पहुंच नहीं हो जाती –
क्या इमारतें और क्या बड़े-बड़े होटल ।
कुर्सी मेज़ों पर खाने उड़ाता है ।
कोई कान तक नहीं देता था जिनकी और
अब देखिए औकात उनकी –
कितना बड़ा अभिनेता हो गया है –
निकल निकल भोंपुओं से
कैसा रंग जमाता है ।
उसके दर्दीले ठुमकों पर
पूरी दुनिया नागिन सी झूमती है ।
हमारा दर्द
जो हमें भिखारी तक बना देता था
पहुंचते ही मंचों पर
हमें दाता की मुद्रा में ला देता है ।
और कवच ओढ़े हमारे दर्दों के वे
(जिनके नाम लेने तक में खतरा
है हमें )
हमारी त्रासदी के देवता बन बॆठते हैं ।
और हम ?
हमें तो पता ही नहीं चलता
कब क्या हो जाते हैं हम ।
हां, गाहे-बगाहे
जाने क्यों लगता है लगने
कि उनके भोंपू ही नहीं अन्दोलन भी
लादे अपने कंधों पर
उन्हें ही ढोते हैं ।
ढ़ोते हैं जैसे ढोते रहे हैं अपनी मजबूरियां
अपनी भूख और प्यास भी
और डरों में लिपटा अपना गुस्सा भी ।
क्या नहीं है यह भी हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी ?
हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी तो यह भी है
कि ताक़त है हममें
पर जीते हैं ताक़त की मुद्रा में ।
हममें युद्ध है
पर जीते हैं युद्ध की मुद्रा में ।
गुस्सा है
जीते हैं गुस्से की मुद्रा में ।
फेंक सकते हैं उखाड़ कर
जीते हैं उखाड़ फेंकने की मुद्रा में ।
समझ है
जीते हैं समझ की मुद्रा में ।
समय की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यह भी है
हम महज बहस करते हैं
वे उलझाए रखते हैं हमें बहसों में जिन्हें वे आश्वासन कहते हैं
मरने का इंतज़ार करते हैं
एक दिन हम सचमुच मर जाते हैं –
उनके धैर्य पर अपने अधैर्य को कुर्बान कर देते हैं
इच्छा उन्हीं की होती है ऎसी, पर अदृश्य ।
महज मुद्रा में होते हैं बहस की, कहां समझ
पाते हैं !
कर
पाते हैं तो बस इतना ही –
फिर बनते रहिए बेवकूफ
जाता है अपने बाप का भी ।
पृथ्वी
उठता चला गया
तूफान !
सीने से
अपने सीने से
नहीं,
कहीं
सा ।
हुआ और खो गया
ही क्या खोने को पर खो गया
दिए गए किसी बच्चे की ज़िद सा ।
आकाश मुझमें डूब गया था
पूरा ।
रहा हाथ-पांव
आकाश हिलोरे ।
चढ़ बॆठा आकाश के कंधों पर ।
मिली
मेरा पिता हो ।
किया
किया पृथ्वी को
मेरे पैरों से ।
ही कब थी वह ।
किया
करने के लिए
रहा सुख औपचारिकता का
रहा याद को,
रुलाता रहा ।
था न मॆं !
से देखा मुझे याद ने
आया था उसका
छुआ ।
वृक्ष पर बॆठी
दिवंगत माँ
निहार रही थी
।
चटका और अपने से दूर हो गया
करीब
गया ।
गुनगुनाता रहा देर तक
बिछी पृथ्वी की गोद में ।
हो पृथ्वी
टहनी पर अटकी हो
पांवों को
माँ ।
फ़रिश्ता तो नहीं था
बाद
आने लगें तो क्या करें?
सड़ांध से
लगें बदबू?
लगें पत्र भी
चुकों की
मानसिकताएं?
दें विवश
खूबसूरत
प्रतीक्षाएं,
पत्रों की
पत्र जब
लिखे हों संपादकों, आलोचकों को)
अगर अपनी सतहों पर
हुए अहंकार
उपेक्षाओं की मार,
दुराग्रह,
कुछ प्रचलित भ्रष्टाचार
करें?
एक समय के बाद
घरों में?
पड़ता है
को भी चिता पर!
फ़रिश्ता तो नहीं था न ?
कबूतर
दिनों से रहा है कबूतर
एक कोने में
की ।
परिवार भी
फड़फड़ा लेता है पंख ।
थमा रह जाता है
में
आस-पास ।
बतिया रहा था कबूतर
पर
से ।
से सुना
चलते समय-
हमारे घर” ।
मुझे अच्छा लगा था
लीजिए चाहे बाकी सब गप्प
लगा था
हमारा है
कबूतर का भी ।
नहीं है अभी अनशन पर खुशियां
बहुत महंगा है और दकियानूसी भी
पर खेलना चाहिए खेल पृथ्वी पृथ्वी भी
कभी कभार ही सही,
किसी न किसी अन्तराल पर ।
हिला देना चाहिए पूरी पृथ्वी को कनस्तर सा,
खेल खेल में ।
और कर देना चाहिए सब कुछ गड्ड मड्ड हिला हिला कर कुछ ऎसे
कि खो जाए तमाम निजी रिश्ते, सीमांत,
दिशाएं और वह सब
जो चिपकाए रख हमें, हमें नहीं होने
देता अपने से बाहर ।
लगता है या लगने लगा है या फिर लगने लग जाएगा
कि कई बार बेहतर होता है कूड़ेदान भी हमसे (और शैली है महज ‘हमसे‘)
कम से कम सामूहिक तो होती है सड़ांध कूड़ेदान की ।
हम तो जीते चले जाते हैं अपनी अपनी संड़ांध में
और लड़ ही नहीं युद्ध तक कर सकते हैं
अपनी अपनी सड़ांध की सुरक्षा में ।
क्या होगा उन खुशबुओं की फसलों का
और क्या होगा उनका जो जुटे हैं उन्हें सींचने में,
लहलहाने में ।
ख़ैर है कि अभी अनशन पर नहीं बैठी हैं ये फसलें खुशबुओं की
कि इनके पास न पता है जन्तर मन्तर का और न ही पार्लियामेंट स्ट्रीट
का ।
गनीमत है अभी ।
बहुत तीखा होता हे सामूहिक खुशबुओं का सैलाब और तेज़ तर्रार भी
फाड़ सकता हे जो नासापुटों तक को ।
डराती नहीं खुशबुएं सड़ांध-सी
पर डरती भी नहीं ।
आ गईं अगर लुटाने पर
तो नहीं रह पाएगा अछूता एक भी कोना खुशबुओं से ।
उनके पास और है भी क्या सिवा खुशबुएं लुटाने के !
बहुत कठिन होगा करना युद्ध खुशबुओं से
बहुत कठिन होगा अगर आ गईं मोरचे पर खुशबुएं ।
खुशबुएं हमें हम से बाहर लाती हैं ।
खुशबुएं हमसे ब्रह्माण्ड सजाती हैं ।
खुशबुएं हमें ब्रह्माण्ड बनाती हैं ।
खुशबुएं महज खुशबू होती हैं ।
खुशबुएं हमें पृथ्वी पृथ्वी का ख़तरनाक खेल खिलाती हैं
और किसी न किसी अन्तराल पर
हमें एकसार करती हैं । हिलाती हैं ।
गनीमत है कि अभी अनशन से दूर हैं हमारी खुशबुएं ।
गाँव किराड़ी (दिल्ली),
28 अगस्त 1946
प्रकाशित रचनाएं:
रास्ते के बीच,
खुली आँखों में आकाश, हल्दी-चावल और अन्य
कविताएं, छोटा
हस्तक्षेप,
फूल तब भी खिला होता, गेहूं घर आया है,
वह भी आदमी तो होता है, बाँचो
खंड-खंड अग्नि (अंग्रेजी,
गुजराती, मराठीऔर कन्नड़ में अनूदित भी ) ।
नये कवियों के काव्य-शिल्प सिद्धान्त, कविता के बीच से,
साक्षात त्रिलोचन,
विवाद भी ।
निषेध के बाद,
हिदी कहानी का समकालीन परिवेश, बालकृष्ण भट्ट,
प्रतापनारायण मिश्र, कथा-पड़ाव ।
कविता-यात्रा,
सुनो अफ्रीका,कोरियाई बाल कविताएं आदि।
सौ एक बाल कविताएं’
और ‘समझदारहाथी:समझदार चींटी’ सहित 15 बाल-कविता संग्रह, आठ
कहानी-संग्रह, लोकथाओं/कथाओंकी ’जादुई
बांसुरी और अन्य कोरियाई कथाए’ सहित 4
पुस्तकें, बाल-नाटक: बल्लू हाथी काबालघर, संस्मरण: फूल भी और फल भी ।
पुरस्कार-सम्मान: सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, गिरिजाकुमार माथुर स्मृति राष्ट्रीय
तथा बाल-साहित्य कृति पुरस्कार,गौरव सम्मान (पोर्ट ऑव स्पेन),
इंडो रशियन लिटरेरी सम्मान, कोरियाई दूतावास
का प्रशंसा-पत्र, भारतीय बाल-कल्याण संस्थान कानपुर का सम्मान,
प्रकाशवीर शास्त्री विशिष्ट सम्मान,
का राष्ट्रीय बाल-साहित्य पुरस्कार, रत्न शर्मा स्मृति
राष्ट्रीय बाल-साहित्य पुरस्कार, भारतीय अनुवाद परिषद,
दिल्ली का द्विवागीश पुरस्कार, ब्लोगोत्सव-2010
कवि सम्मान ।
बी-295,
सेक्टर –20, नोएडा-201301, मो- 9910177099 divik_ramesh@yahoo.com



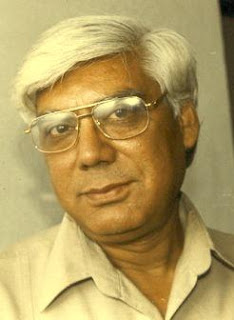
bahut sashakt rachnaen..