जांठि को घुङुर / दिवा भट्ट
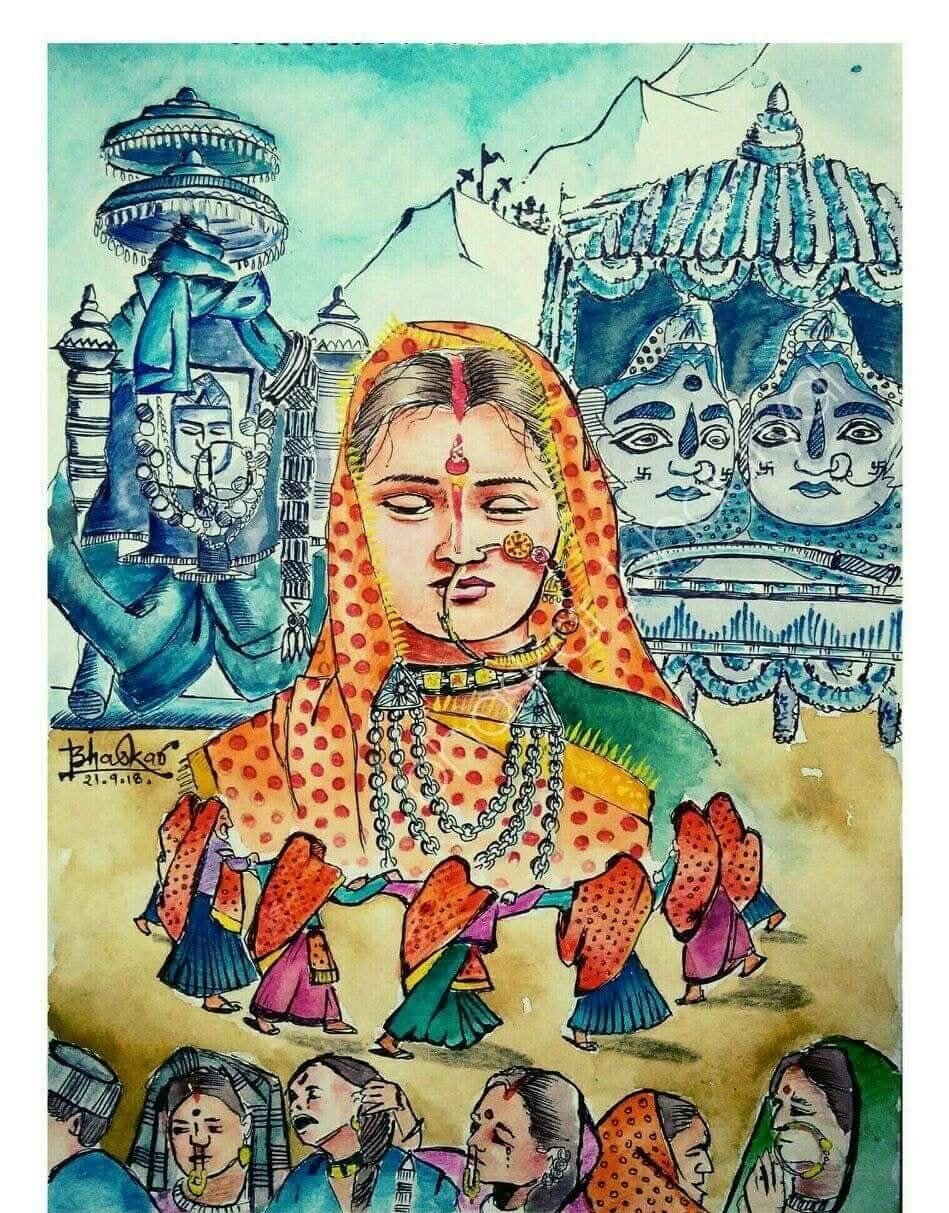
जांठि को घुङुर,
कै थें कूनूं दुखि-सुखि, को दिलो हुंङुर।
(लाठी का घुंघरु (बजता है)
मैं किससे कहूं अपने सुख-दु:ख, कौन देगा हुंङुर)।
यह कुमाउनी लोकगीत न्योली का एक त्रिपदीय दोहा है। हिंदी दोहे की भांति कुमाउनी के लोक छंद दोहे; जिसे जोड़ या कभी न्योली भी कहा जाता है; के भी चार चरण होते हैं, किंतु इसके दो भेद हैं; तृपदीय और चतुष्पदीय। उपर्युक्त तृपदीय दोहे की प्रथम पंक्ति में एक चरण है तथा दूसरी में दो।
हुंङुर अर्थात् किसी की बात ध्यान से सुनते हुए हूंऽ-हूंऽ या हॅं-ऽ हॅं ऽ कहते हुए उसे अपनी सहानुभूतिपूर्ण उपस्थिति की प्रतीति कराना। यह भरोसा दिलाना कि मेरे कान खुले हैं तुम्हारी बात सुनने के लिए। कान ही नहीं; मेरी संपूर्ण चेतना सजग और उत्सुक है तुम्हारी बात सुनने-समझने के लिए। कहने वाले को सुनने वाले कान चाहिए। मात्र शब्दों और ध्वनियों को ग्रहण करने वाले कान नहीं; बल्कि शब्दों की ध्वनियों के भीतर की गहराई से तरंगाइत होने वाली संवेदनाओं को समझने वाले ऐसे कान; जिनके साथ चित्त भी सम्मिलित है। हुंङुर का अर्थ केवल स्वीकृति सूचक ‘हां’ नहीं है। यह ऊंचे स्वर में बोले जाने वाला ‘हां- हां’ भी नहीं है। यह मंद्र सप्तक सुरों की भांति छाती के भीतर से धीरे-धीरे ऊपर को उठने वाली एक धीमी- सी गूंज है; जो कहती है! ‘हां- हां, कहो, मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं। तुम्हारे सुख-दुख, संघर्षों-उपलब्धियों और विशिष्ट अनुभवों में मैं तुम्हारे साथ हूं।’
वक्ता को श्रोता की आवश्यकता होती है, लिखने वाले को पाठक की और दृश्य कला को दर्शक की। अभिव्यक्ति की सार्थकता इसी में है कि वह अन्य तक पहुंचे तथा अन्य द्वारा समझी जाए। यही सार्थक संप्रेषण है। केवल कह देने मात्र से संप्रेषण पूरा नहीं हो जाता। तीर अगर धनुष से निकला है तो उसको लक्ष्य तक पहुंचना ही चाहिए, अन्यथा उसका चलना व्यर्थ है। शब्द, चित्र, मूर्ति, नृत्य या अभिनय इत्यादि दृश्य अथवा श्रव्य किसी भी माध्यम से की जाने वाली अभिव्यक्ति का उद्देश्य यही है कि वह सामनेवाले के हृदय तक पहुंचे। इसी तथ्य को परिभाषित और व्याख्यायित करने के लिए प्राचीन काल से अब तक अनेक मत, अनेक सिद्धांत और अनेक शास्त्रीय ग्रंथ प्रकट हो चुके हैं; फिर भी लोक के अनाम निरक्षर व्यक्तियों द्वारा की गई इस सरल-सीधी अभिव्यक्ति का चमत्कार देखिए कि डेढ़ पंक्ति के इस दोहे में अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण का गहन अर्थ सहज ही उद्घाटित हो गया है।
मनुष्य जब से भाषा में अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति करने लगा तभी से उसे किसी सुनने वाले की प्रतीक्षा रही है। केवल अपने सुख -दु:ख व्यक्त करने के लिए ही नहीं; अपना ज्ञान, मंतव्य और विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी किसी सुपात्र की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने आत्मीय के सम्मुख अपनी गलतियों और कमजोरियों का स्वीकार कर सही राय लेने के साथ – साथ अपने हृदय के भार को हल्का भी करता है। इसी प्रकार वह अपने आत्मीयों की गलतियों के लिए उन्हें रोकता – टोकता है और आवश्यक होने पर उचित राय भी देता है। कह सकते हैं कि मनुष्य को अपने सुख -दुख व्यक्त करने के लिए ही नहीं; उचित दिशा निर्देशों के लिए भी किसी अपने आत्मीय व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कोई सुनना ही न चाहता हो तो?
श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध रोकना चाहते थे, किंतु नहीं रोक पाये। उन्हें भी कहना पड़ा था; ‘उर्ध्व बाहुर्वदाम्यहम् न कश्चित्श्रृणोति मे।’ अर्थात् मैं बांहें उठा-उठाकर कह रहा हूं, लेकिन कोई मुझे नहीं सुनता। ‘न कश्चित्श्रृणोति मे’ की पीड़ा बड़ी गहरी होती है। 20वीं शताब्दी के विश्व युद्धों के समय जब शांति की बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था; तब अंतरराष्ट्रीय मानवतावाद में आस्था रखने वाले प्रसिद्ध लेखक हेमिंग्वे ने ‘फोर हूम द बेल टोल्ड्स्’ लिखा था। इस तरह के उद्गारों में यही पीड़ा मुखरित होती है कि कौन सुन रहा है हमें? किसके लिए कह रहे हैं हम?
केवल सुख- दुःख के अनुभव ही नहीं; व्यक्ति किसी विचित्र, अटपटे और नये अनुभव को भी अकेले नहीं पचा पाता। उन्हें किसी अन्य को बताए बिना उसे चैन नहीं मिलता। ‘राजा के सिर में सींग’ नामक लोक कथा इसी अनुभव की ओर संकेत करती है।
एक राजा के नाई के बीमार हो जाने पर उसके स्थान पर उसका बेटा बब्बन राजा की हजामत बनाने जाता है। राजा की हजामत बनाते समय उसे पता चलता है कि राजा के सिर में सींग है। इस विचित्र बात को मन में छिपाकर रखना उसके लिए कठिन हो जाता है। किसी अन्य को बताने पर प्राण दंड का भय है और यह गुप्त रहस्य किसी को बताए बिना रह भी नहीं पाता। अंततः वह जंगल में जाकर एक पेड़ के सामने यह रहस्य उगल आता है। पेड़ को सुना कर वह खुद तो भार- मुक्त हो गया, लेकिन यह विचित्र बात पेड़ को भी भारी लगने लगी। उसने वह एक हिरण को बता दी। हिरण किसी अन्य को बताता, उससे पहले एक शिकारी द्वारा उसका वध कर दिया गया। बाद में उसकी खाल से मृदंग बना। मृदंग जब राज दरबार में बजाया जाने लगा तो उसके ताल से जो ध्वनि गूंजी; वह थी; ‘सींग- सींग, बब्बन- बब्बन। सींग- सींग, राजा के सिर पर सींग।’
यह लोक कथा बताती है कि विशिष्ट अनुभवों को अकेले अपने मन में रखना कितना कठिन है और उन्हें कह देने से किस तरह मुक्ति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि सत्य कभी छिपता नहीं; कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है।
जिनके पास उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता अथवा कोई होते हुए भी अनसुना कर देता है; उनका कथन अधूरा ही नहीं रहता; वरन निरर्थक भी हो जाता है। कुमाउनी भाषा में इसके लिए भी एक कहावत है ; “अॅं कूण बिगर काथ् अटकी रै।” अर्थात् ‘हां’ या ‘हूं’ के रूप में प्रत्युत्तर न मिलने के कारण कथा ही अधूरी रह गई है, अकथित रह गई है। किससे कहें? कौन सुनेगा? इस अपेक्षा और प्रतीक्षा पर हिंदी में भी सैकड़ों गीत-काव्य बने हैं:
“माई री! मैं का से कहूं पीर अपने जिया की।”
“किसको सुनाएं दास्तां, किसको दिखाएं दिल के दाग।”
“तुम जो न सुनते क्यों गाता मैं।”
“कौन आएगा यहां, किसकी राह देखें हम।”
“हाले दिल हमारा जाने न कोई “
“कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा।”
कवि नीरज भी कह गए हैं: “कौन खरीदेगा तेरे घायल आंसू दो-चार।”
प्रश्न यह है कि कोई अपने हृदय के भावों को क्यों दूसरों से कहना चाहता है? क्या इससे उसके दु:ख मिट जाते हैं? क्या इससे उसकी समस्याओं का निराकरण हो जाता है? क्या इससे उसका सुख बढ़ जाता है? घटनाएं तो अपने क्रम से घटती रहती हैं। समस्याएं अपनी जगह खड़ी रहती हैं। उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन उन्हें किसी अन्य के सम्मुख व्यक्त कर देने से प्रभावित व्यक्ति के मन- मस्तिष्क पर लदा हुआ दु:ख अथवा समस्या का भार हल्का हो जाता है। समस्याओं का निदान दिखाई देने लगता है, सहिष्णुता बढ़ने लगती है और अपने ही भीतर से एक ऊर्जा का संचार होता अनुभव होता है, जो भीषण कष्ट को भी सरल बना देता है। एक व्यक्ति की भावाभिव्यक्तियों को सुनकर दूसरा व्यक्ति उनसे मुक्ति का उपाय न भी बताएं; केवल ‘हॅं’ –‘हॅं’ करता हुआ उन्हें सुनता ही भी रहे; तो उतने से ही भी वक्ता का मनोबल बढ़ता है कि हम अकेले नहीं हैं, निराधार नहीं हैं। कोई हमारे साथ है। यह भरोसा ही हृदय को भार मुक्त करता है और मस्तिष्क को कष्ट निवारण के उपाय सुझाने लगता है।
अपने सुखात्मक या दु:खात्मक अनुभवों को व्यक्त करना जीव मात्र का स्वभाव होता है, किंतु उनके माध्यम और प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं। मनुष्येतर प्राणी भी अपने प्रिय-अप्रिय भावों की अभिव्यक्ति किसी न किसी भंगिमा में करते ही हैं। मनुष्य को इन अभिव्यक्तियों के लिए किसी अन्य सहृदय की भी आवश्यकता होती है। खुशी में वह अकेले हंसे या दुःख में अकेले रोए तो वह अटपटा असामान्य प्रतीत होगा। ऐसा करने वाला मनुष्य पागल कहलायेगा। किसी अन्य की उपस्थिति के बिना ऐसा एकालाप अभिव्यक्ति की सार्थकता का अनुभव नहीं होने देता।
अनुभव साझा करने से एक के मन का भार घट जाता है; तो दूसरे का भी ज्ञान बढ़ता है तथा जीवन को जीने और समझने की नई दृष्टि विकसित होती है। मनुष्य वह प्राणी है, जो दूसरों के अनुभवों से सीखता है। उनकी उपलब्धियों के साथ -साथ उनकी गलतियों से भी सीखता है। सुख- दुःख, भय, क्रोध, आश्चर्य तथा घृणा इत्यादि विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति स्वाभाविक एवं आवश्यक है। कह देने से उनके विपरीत प्रभाव की सघनता कम हो जाती है और सकारात्मक अनुभव प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। इसीलिए लोग मित्र बनाते हैं तथा सगे-संबंधियों से मिलजुल कर सुख-दुख बांटते हैं। दुःखी व्यक्ति को रोने के लिए किसी अपने के कंधे की आवश्यकता होती है, अर्थात् दुःख की घड़ी में किसी आत्मीय व्यक्ति की निकटता और सहानुभूति औषधि की भांति मन के घावों को भर देती है।
एक पथिक के हाथ की लाठी उसकी सहयात्री होती है। चलते समय उसमें बंधे हुए घुंघरू भी बजने लगते हैं। लाठीधारी व्यक्ति घुंघरुओं की लय के साथ बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। उसे अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं चल रहा है। लाठी उसके साथ है, घुंघरू उसके साथ हैं। उस सांगीतिक गति के साथ चलते हुए थकान महसूस नहीं होती। चलना संगीतमय अर्थात् आनंदमय बन जाता है। इसी तरह घुंघरुओं की ध्वनियों को कोई सुन रहा है, उनसे आनंदित हो रहा है तो घुंघरुओं का आनंद भी बढ़ जाता है और वे भी अधिक सुमधुर ध्वनि में बजने लगते हैं। घुंघरू का इस तरह झंकृत होना भी हुङुर लगाने के समान है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के अनुभवजन्य संवेदनों को सुनने- समझने- सहलाने वाला दूसरा व्यक्ति भी उसे उद्वेलित हुए बिना धैर्य पूर्वक आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है।
हृदय को सकारात्मक अथवा नकारात्मक किसी भी प्रकार से उद्वेलित करने वाले अनुभवों का सार्थक संप्रेषण मनुष्य जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है; यह बात यहां प्रयत्न पूर्वक शास्त्रीय शब्द खोज कर नहीं कही गई है। यह तो लोक हृदय के अंत:स्थल से निकली हुई सहज अभिव्यक्ति है; जो अपनी सरलता, गहनता, मर्मस्पर्शिता और संप्रेषण की अद्भुत क्षमता की प्रतीति कराती हुई प्रेरित भी करती है कि किसी के मुख बनो तो किसी के श्रवण भी बनो। उन्हें हुंङुर दो। कहने और सुनने से हृदय का विरेचन होता है, प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और अनुभवजन्य ज्ञान का प्रसारण जीवन यात्रा का पाथेय बन जाता है।
हमारे लोक साहित्य में चमत्कृत करने वाले ऐसे एक से बढ़कर एक हजारों मुहावरे- लोकोक्तियां और काव्य पंक्तियां विद्यमान हैं। उन्हें गहराई में जाकर समझेंगे तो लोक साहित्य में निहित कलात्मकता, ज्ञान संचयन तथा लोक भाषा की अद्भुत अभिव्यक्ति क्षमता का आनंद भी प्राप्त होगा ।
***